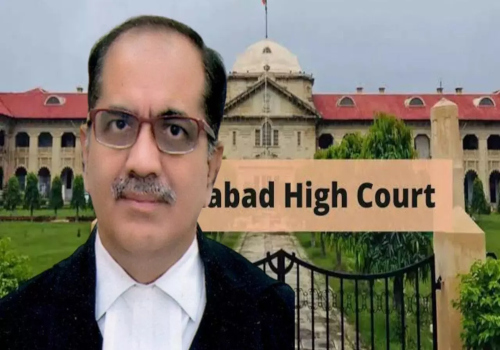आइएससी ( इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ) के एक सर्वेक्षण में यह बात निकल कर आयी है कि जनवरी 2025 में भारत में इंटरनेशनल स्कूलो की संख्या 972 है जबकि 2019 में इनकी संख्या 884 थी. पांच सालों में इनमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई. लोगों का कहना है कि भारत में संपन्नता बढ रही है तो संपन्न लोग अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में भेजना चाहते हैं. इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि देश में जब 80 फीसदी लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं तो जो संपन्नत बढ़ रही है वह शेष 20 फीसदी लोगों की बढ़ रही है और उन्हीं बीस प्रतिशत लोगों के बच्चों के लिए ये सब आयोजन हो रहे हैं, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है.
भारत का संविधान शिक्षा का अधिकार देता है. देश के सभी बच्चों को एक समान शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व भारत सरकार पर है. आजादी के पहले से ही क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारत में स्कूल खोलकर शिक्षा का प्रचार करना शुरू कर दिया था. उस समय यह सेवा भाव से किया गया होगा. लेकिन आजादी के बाद बेहतर शिक्षा व्यवस्था के नाम पर शुल्क लेकर पढ़ाना शुरु किया.
भारत में शिक्षानीति बनाने का काम केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा होता है. इसी नीति को आधार बना कर पाठ्यक्रम , सिलेबस और शिक्षा का माध्यम तय होता है. इसी के तहत केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड का गठन होता है जिसे सीबीएससी बोर्ड भी कहा जाता है. यह बोर्ड दसवीं और बारहवी कक्षा के बोर्ड परिक्षाओं का संचालन करती है. इसके अलावा केन्द्र सरकार के द्वारा ही केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है जो देश के कई शहरों में सीबीएससी पाठयक्रम के तहत चलाये जाते है. केद्रीय विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल तथा इंजनीयरिंग कालेज भी केंद्र सरकार संचालित करती है.
देश के प्रत्येक राज्य में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी होती है. इस लिए प्रत्येक राज्य की सरकार प्रथम कक्षा से लेकर बारहवी कक्षा तक की पढ़ायी के लिए स्कूल खोलती है. इनके संचालन की जिम्मेदारी राज्य के शिक्षा विभाग की होती है जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है. राज्य सकारों का अपना शिक्षा बोर्ड होता है जो दसवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करती है. राज्य के अपने विश्वविद्यालय और कालेज भी होते हैं.
आजादी के बाद देश भर में इसी व्यवस्था के तहत स्कूली शिक्षा को निःशुल्क बनाया गया, ताकि गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिले. लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में आर्थिक उन्नति होती गयी लखपतियों और अरब पतियों की संख्या भी बढती गयी. और मोटा वेतन पानेवाला सरकारी कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग भी बन गया जिन्हें सरकारी स्कूलों की पढ़ाई जंची नहीं. उन्हें लगा कि उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर्याप्त नहीं है.
तो ऐसे लोग पहले मिशन स्कूलों की ओर आकर्षित हुए जो तब तक लाभ कमाने वाली शिक्षण संस्थायें बन चुकी थी. इसके साथ ही कई अन्य निजी शिक्षण संस्थाएं भी वजूद में आयीं जो गुणवत्ता युक्त शिक्षण का लेबल लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में उतरीं जिनका ध्येय मोटी शुल्क के द्वारा लाभ कमाना था. इसका एक कारण यह भी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर उसका रख -रखाव व्यवस्था आदि में बहुत गिरावट भी आती गई. इसके लिए हम केवल शिक्षकों को ही जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं. इसमें सरकार की गैर जिम्मेदारी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के प्रति उदासीनता भी कारण रहा है.
इसलिए धडल्ले से प्राइवेट स्कूल खुलने लगे. अब थोडी बहुत हैसियत वाले मां बाप भी अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए लालायित रहने लगे. ये प्राइवेट स्कूल सीबीयससी शिक्षा बोर्ड के तहत उसके पाठयक्रम को अपनाकर शिक्षण कार्य करते है. सीबीएससी शिक्षा बोर्ड की मान्यता विदेशों में भी है.
लेकिन हमारे देश के नवधनाढ्य लोग तथा अरबपति नेताओं की महत्वाकांक्षा का यहीं अंत नहीं होता है. उनकी श्रेष्ठ संतानों के लिए भारत के ये प्राइवेट स्कूल भी उपयोगी नहीं रहे. क्योंकि उनका ध्येय होता है कि उनके बच्चे उच्चशिक्षा विदेशों में ही प्राप्त करे. तब सोचा गया कि विदेशी स्कूलों के पाठ्यक्रम को लेकर उनकी पद्धति से पढ़ाकर वहां की शिक्षा बोर्ड की परीक्षा को संचालित करने वाले स्कूलों की स्थापना भारत में क्यों न हो. इच्छा हो तो यह कार्यरूप में भी परिणत होता है. अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खुल गये. विभिन्न नामों के इंटरनेशनल स्कूल भारत में खुलने लगे. जो एलिट वर्ग की शैक्षणिक जरूरत को पूरा करते हैं. सीएआइई बोर्ड (जो कैंब्रिज विश्वविद्यालय से जुडा है ) तथा आइबी बोर्ड विदेशी पाठ्कम के अनुसर वहां की शिक्षण पद्धति के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं. इन्हीं बोर्डों के द्वारा इंटरनेशल स्कूल चलते हैं जहां पढ़ने वाले बच्चे विदेशी उच्च शिक्षा के काबिल बनते हैं.
सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि केंद्र तथा राज्य सरकारों को अपने बजट में शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ा देना चाहिए. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा मद में अवंटन बढ़ा देने से ही सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जायगी. सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी. सामूहिक प्रयास है तो सामूहिक जिम्मेवारी निश्चित हो और उसके अनुसार कार्य प्रणाली बने. अन्यथा इस ओर उदासीन और इच्छा रहित सरकार कुछ नहीं कर पायेगी. शिक्षा के लिए बढ़ाया गया मद या तो अनुपयोगी रह जायगा या भ्रष्टाचार को बढ़ायगा. सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय निजी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों को जगह और अनुदान देकर उनकी सहायता कर रही है. ऐसी स्थिति में भारत में तीन तरह की शिक्षा व्यवस्था बनी रहेगी और समान शिक्षा व्यवस्था सपना बन कर ही रह जायगी.